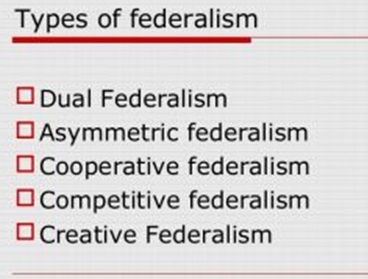प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी, संघवाद, असममित संघवाद, अनु. 370, अनु. 371
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर- 2 |
चर्चा में क्यों-
- 1 दिसंबर, 2023 को दिए गए अपने निर्णय में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने असममित संघवाद को भारतीय संघ के एक भाग के रूप में परिभाषित किया। इसमें संघीय उप- इकाईयों (राज्यों) के बीच कुछ विभेदक अधिकार शामिल हैं। पीठ ने असममित संघवाद की व्याख्या बुनियादी ढांचे के रूप में किया है।
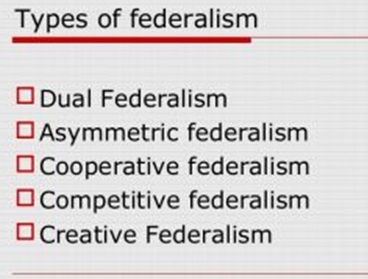
मुख्य बिंदु-
- संविधान किसी राज्य के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं प्रदान करके विशिष्ट समस्याओं को समायोजित करता है।
- फैसले में कहा गया है कि असममित संघवाद के कारण एक विशेष राज्य कुछ हद तक स्वायत्तता का लाभ उठा सकता है, जबकि दूसरा राज्य नहीं।
- यह अंतर केवल स्तर का है न कि प्रकार का।
- संघीय व्यवस्था के तहत अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग लाभ मिल सकते हैं लेकिन सामान्य सूत्र संघवाद है।
भारतीय संघ की विशेषता-
- संवैधानिक रूप से भारत की शासन संरचना अर्ध-संघीय है।
- एकात्मक व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति केंद्र में निहित होती है, किंतु संघीय ढांचे में महासंघ बनाने वाली इकाईयों के पास अपने मामलों के संचालन के लिए स्वायत्तता और शक्तियों की अलग-अलग डिग्री होती है।
- भारतीय संदर्भ में यद्यपि राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है, किंतु संविधान कुछ क्षेत्रों में केंद्र की ओर झुकता है. इस प्रकार यह व्यवस्था इसे अर्ध-संघीय बनाता है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ शामिल हैं जो उन विषयों को निर्धारित करती हैं जिन पर केंद्र और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है।
- समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून लागू होगा।
असममित संघवाद-
- इस प्रकार के संघवाद में राजकोषीय, राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध असमान शक्तियों पर आधारित होते हैं। इसे दो प्रकार से देखा जा सकता है-
-
- संघ की व्यवस्थाओं के बीच उर्ध्वाधर विषमता - केंद्र और राज्यों के बीच
- संघ की व्यवस्थाओं के बीच क्षैतिज विषमता - राज्यों के बीच
- असममित संघवाद के विरुद्ध एक तर्क दिया जाता है कि तथाकथित विशेष स्थितियाँ क्षेत्रवाद और अलगाववाद के बीज बोती हैं और यह राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती हैं।
- अनुच्छेद 370 को असममित संघवाद का सबसे स्पष्ट उदाहरण माना जाता है, किंतु भारत में ऐसे कई अन्य राज्य हैं जो अलग-अलग स्तर की स्वायत्तता और केंद्र के साथ संबंध का लाभ उठाते हैं।
- असममित व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान में हो,यह आवश्यक नहीं। ऐसी व्यवस्थाएं किसी संघ में प्रशासनिक, राजनीतिक और राजकोषीय प्रणालियों को लागू करने के तरीके से भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- भारत के संविधान निर्माताओं ने शासन के लिए ‘सलाद कटोरा दृष्टिकोण’ (salad bowl approach) की आवश्यकता को पहचाना जो देश में विशिष्ट सांस्कृतिक अंतरों को पहचानता है और साझा शासन की योजना के अंतर्गत स्व-शासन की अनुमति देता है।
संवैधानिक प्रावधान-
1. ऊर्ध्वाधर विषमता-
-
- भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान है।कुछ विशेषताओं में शामिल हैं-
-
- अनुच्छेद 3- केंद्र राज्य के नाम और सीमाओं में एकतरफा बदलाव कर सकता है।
- अनुच्छेद 352 एवं 356- राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित प्रावधान।
- अनुच्छेद 248- कानून की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं।
2. क्षैतिज विषमता
- अनुसूची 4- राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है। राज्य परिषद में उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 सीट है।
- भाग VIII- भारतीय संविधान के भाग VIII में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान, जिनकी संघीय व्यवस्थाएं राज्यों की तुलना में भिन्न हैं।
- अनुसूची 5- संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के साथ-साथ किसी भी क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा अन्य राज्य।
- अनुसूची 6- संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान हैं। ये स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र बनाते हैं।
- अनुच्छेद 371 एवं अन्य: अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्छेद 371जे तक, यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान देता है।
3.राजकोषीय विषमता-
-
- वित्त आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी (ऊर्ध्वाधर विषमता)- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2021-26 अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की अनुशंसा की गई।
- राज्यों के बीच हस्तांतरण (क्षैतिज विषमता)-15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों में करों के हस्तांतरण के लिए उनके बीच आय असमानता, जनसंख्या कम करने के लिए किए गए प्रयास, वन और पारिस्थितिकी आदि जैसे मानदंडों का उपयोग किया गया।
- अनुदान- 2021-26 की अवधि में चयनित राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान किए गए।
केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) वे योजनाएँ हैं, जिसमें केंद्र के साथ- साथ राज्य की भी भागीदारी है।
- यह फंडिंग केंद्र तथा राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जाती है।
- विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों में यह अनुपात 90:10 का होता है।
जम्मू, कश्मीर का मामला-
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जम्मू और कश्मीर में विशेष परिस्थितियों के कारण एक विशेष प्रावधान की आवश्यकता है, जो कि अनुच्छेद 370 है और यह असममित संघवाद का एक उदाहरण है।
- संवैधानिक संरचना में कुछ एकात्मक विशेषताएं मौजूद हैं, जिनके संदर्भ में केंद्र सरकार के पास कुछ स्थितियों में अधिमानी शक्तियां हैं, किंतु संविधान द्वारा राजव्यवस्था की आधारशिला में संघीय तत्वों का अस्तित्व है।
- पीठ के अनुसार, "इस व्यवस्था को अर्ध-संघीय, असममित संघवाद या सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया है।"
- न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के अनुसार, जम्मू और कश्मीर ने भारत में शामिल होने और असममित संघीय मॉडल के भीतर स्वायत्तता पर बातचीत करने का निर्णय लिया था।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग वैध कैसे पाया गया? इसका जवाब असममित संघवाद और संप्रभुता के बीच सूक्ष्म अंतर में निहित है।
- पीठ ने पाया कि जम्मू-कश्मीर राज्य ने विलय पत्र (आईओए) के क्रियान्वयन और 25 नवंबर, 1949 की उद्घोषणा जारी होने के बाद संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा, जिसके द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था।
- पीठ ने स्पष्ट किया, "जम्मू और कश्मीर राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग है।
बुनियादी ढांचा में खतरा-
- पीठ ने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की कि "आंतरिक संप्रभुता" की कमी के कारण जम्मू-कश्मीर असममित संघवाद से वंचित कैसे हो जाएगा, जिसे वह संविधान का बुनयादी ढांचा मानती है।
- ऐतिहासिक और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कोर्ट ने अनुच्छेद 370 एक वैकल्पिक व्यस्था थी
- क्या असममित संघवाद की एक विशेषता के रूप में इसकी निरंतरता को दूर किया जा सकता है, भले ही बुनियादी ढांचे के लिए इसके विनाशकारी परिणामों को नजरअंदाज कर दिया जाए?
- पीठ के अनुसार, अवशिष्ट विधायी शक्तियों को अवशिष्ट संप्रभुता के बराबर नहीं माना जा सकता है।
- पीठ ने कहा, " यह संघवाद के मूल्य और भारत के संविधान के संघीय आधारों को दर्शाता है।"
- जम्मू-कश्मीर के अन्य राज्यों के विपरीत अवशिष्ट विधायी शक्तियां थीं।
- पीठ को आंतरिक संप्रभुता और संघीय विशेषता के बीच यह अंतर करने में न्यायोचित शक्ति है, क्योंकि फैसले में इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि संविधान के इतने महत्वपूर्ण संघीय आधार को पर्याप्त औचित्य के बिना क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए।
- अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं हैं और इस मामले में केंद्र और राज्य समान हैं।
- पीठ का कहना है कि राज्यों का अस्तित्व नागरिकों को शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करता है।
- अनुच्छेद 1 के अनुसार, राज्य देश की संवैधानिक संरचना के लिए आवश्यक और अपरिहार्य हैं और राज्यों के अस्तित्व के बिना संघ का अस्तित्व नहीं हो सकता है।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के गंभीर परिणाम होते हैं, अन्य बातों के अलावा यह राज्य के नागरिकों को एक निर्वाचित राज्य सरकार से वंचित करता है और संघवाद पर आघात करता है।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के अनुसार, किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के परिवर्तन या निर्माण को बहुत मजबूत और ठोस आधार देकर उचित ठहराया जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 3 का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए।
- सिर्फ इसलिए कि अनुच्छेद 370 की कल्पना एक अस्थायी प्रावधान के रूप में की गई थी, क्या असममित संघवाद की एक विशेषता के रूप में इसकी निरंतरता को दूर किया जा सकता है, भले ही बुनियादी ढांचे के लिए इसके विनाशकारी परिणामों की अनदेखी की जाए?
- कानून की इतनी स्पष्ट व्याख्या के बावजूद पीठ ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की वैधता की जांच करने से कतरा गई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वादा किया था कि केंद्र जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करेगा।
प्रतिनिधि लोकतंत्र का ह्रास-
- स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी मौजूदा राज्य को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया है और यदि ऐसा होता है तो प्रतिनिधि लोकतंत्र और संघवाद में कमी आती है।
- संघवाद की भारतीय परिभाषा राज्यों को केवल प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मानने की नहीं है।
- भारत "विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ" का अर्थ यह है कि राज्यों को संसद द्वारा पुनर्गठित किया जा सकता है; लेकिन संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हुए उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है या उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बदला जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संघ को प्राप्त शक्ति - नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित – का उपयोग संसद द्वारा "संघ का संघ" बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा।
- अनुच्छेद 3 के तहत संघ की शक्ति संघवाद के सिद्धांत से टकराती है।
जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों में-
- संविधान का अनुच्छेद 371A से 371Z नौ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाता है।
- ये सभी अपवाद संविधान की "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" नामक धारा के अंतर्गत हैं, जो इंगित करता है कि ये प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक संकट - या तो अलगाववादी भावनाएं या युद्ध - समाप्त नहीं हो जाता।
- "अस्थायी" टैग के बावजूद, किसी भी प्रावधान में स्पष्ट समाप्ति तिथि नहीं है।
- नागालैंड और मिजोरम को बातचीत के आधार पर स्वायत्तता प्राप्त है, जो भारत और नागा एवं मिजोरम स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच एक राजनीतिक समझौता था। इसके तहत, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागाओं और मिज़ोस की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं या उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण में हस्तक्षेप करती हो।
- राजनीतिक आवश्यकताओं के अलावा अन्य कारणों से राज्यों को रियायतें दी गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली पहली अनुसूची के तहत एक राज्य नहीं है, फिर भी सातवीं अनुसूची में राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां हैं।
|
प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-
प्रश्न- असममित संघवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- असममित संघवाद के कारण एक विशेष राज्य कुछ हद तक स्वायत्तता का लाभ उठा सकता है, जबकि दूसरा राज्य नहीं।
- यह अंतर केवल स्तर का है न कि प्रकार का।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर- (c)
मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-
प्रश्न- असममित संघवाद के कारण एक विशेष राज्य कुछ हद तक स्वायत्तता का लाभ उठा सकता है, जबकि दूसरा राज्य नहीं। विवेचना कीजिए।
|

 Contact Us
Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757
New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757
Tech Support : 9555124124/ 7428085757