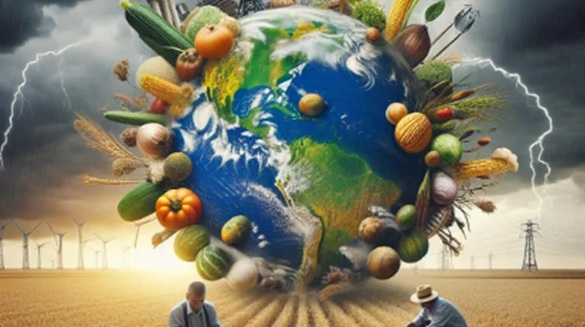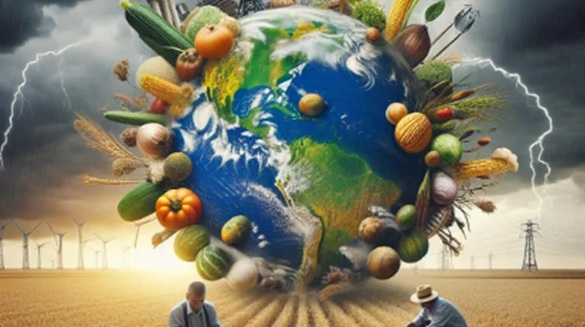
- जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यता के सामने सबसे गंभीर संकटों में से एक है।
- इसके प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह स्वास्थ्य, कृषि, जल-संसाधनों, और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डालते हैं।
- भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनौती यह है कि वह आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखे। इसी दिशा में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ठोस जलवायु कार्रवाई (Climate Action) के संकल्प लिए हैं।
भारत की जलवायु कार्रवाई: एक नज़र में
- भारत, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते, अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के माध्यम से स्पष्ट जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत कर चुका है।
भारत के NDC लक्ष्य (2030 तक)
- 2005 के स्तर की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना।
- गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 50% प्राप्त करना।
- वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO₂ के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।
पंचामृत संकल्प: COP26 ग्लासगो में भारत की प्रतिबद्धता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो (COP26) में भारत की जलवायु कार्रवाई के लिए "पंचामृत" का संकल्प रखा, जिसमें पाँच प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं:
- 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करना।
- 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
- 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय संसाधनों से पूरी करना।
- 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाना।
- 2030 तक 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी करना।
भारत की उपलब्धियां और प्रगति
भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई।
- गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक 46.52% तक पहुँच गई।
- वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से 2005–2021 के बीच 2.29 बिलियन टन CO₂ के बराबर कार्बन सिंक का निर्माण हुआ।
हालाँकि भारत अभी भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर वैश्विक औसत से कहीं कम है।
चुनौतियाँ और मुद्दे
भारत की जलवायु नीति महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कई बाधाएँ हैं:
- नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत।
- कंपोनेंट्स के आयात पर अधिक निर्भरता (विशेषकर सोलर पैनल व लिथियम बैटरी)।
- ग्रिड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन अवसंरचना की सीमाएँ।
- कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने की धीमी गति, जिससे ऊर्जा संक्रमण बाधित होता है।
- नीति और क्रियान्वयन के बीच लगभग 8% का अंतराल, जैसा कि NDC रिपोर्टों से पता चलता है।
भारत की नीतियाँ, योजनाएँ और पहलें
(क) राष्ट्रीय स्तर पर
- राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर (NAPCC)
- राष्ट्रीय अनुकूलन निधि
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018)
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
- ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति
- योजनाएँ: पीएम-कुसुम, पीएम-सूर्य घर, Perform, Achieve and Trade (PAT), उज्ज्वला योजना, FAME India Mission आदि।
(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
- आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)
- LIFE (Lifestyle for Environment) मिशन
(ग) स्थानीय पहलें
- अहमदाबाद नगर निगम के बजट में क्लाइमेट चैप्टर का समावेश।
- गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी।
आगे की राह
भारत के लिए जलवायु कार्रवाई केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि एक संतुलन की नीति है — विकास और स्थायित्व के बीच। आगे की दिशा निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित होनी चाहिए:
- दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और अल्पकालिक ऊर्जा माँगों में संतुलन।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) में निवेश को प्रोत्साहन।
- स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ, जैसे केरल की पचथुरुथु पहल और झारखंड की स्वनिति विकास योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नेट-ज़ीरो ट्रांजिशन के लिए वित्त और तकनीकी सहायता का विस्तार।
निष्कर्ष
- भारत की जलवायु प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि विकासशील देशों में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति मौजूद है।
- भारत का मॉडल “विकास के साथ स्थायित्व” (Sustainable Growth with Equity) पर आधारित है।
- यदि देश अपने वर्तमान मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहा, तो यह न केवल 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका भी निभाएगा।

 Contact Us
Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757
New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757
Tech Support : 9555124124/ 7428085757