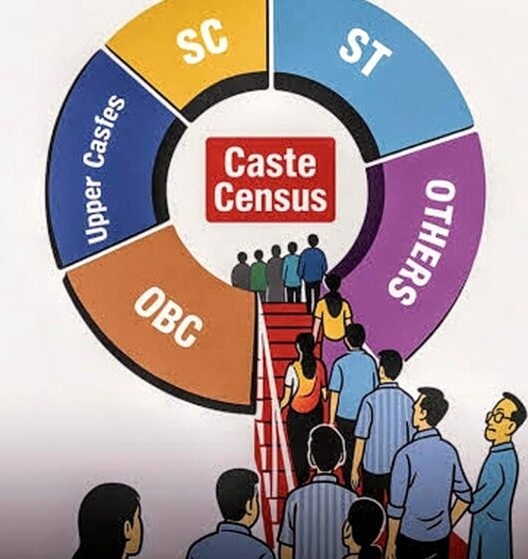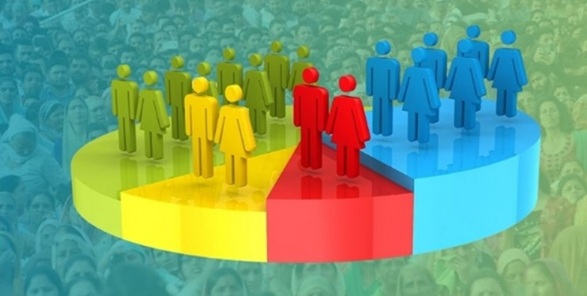भारत में वर्ण व्यवस्था आधारित प्राचीन सभ्यता रही है बाद में ये जटिल जाति (Caste) आधारित सामाजिक संरचना (Social Structure)में परिवर्तित हुई , जिसका असर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक सामाजिक सुधार (Social Reforms) किए, लेकिन जाति आधारित डेटा (Caste-Based Data) का आधिकारिक संग्रह दशकीय जनगणना (Decadal Census) में लंबे समय तक नहीं हुआ।
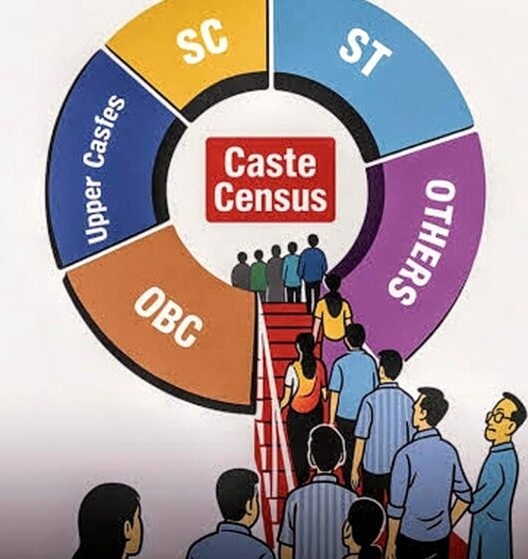
केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी जनगणना (Upcoming Census) के लिए अधिसूचना (Notification) जारी की है। इसके तहत लद्दाख (Ladakh) जैसे हिमाच्छादित (Snow-Covered) क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी, जबकि देश के अन्य भागों में 1 मार्च, 2027 से। इस बार की जनगणना में जातिगत जनगणना (Caste Census) को शामिल किया गया है, जो समाज और नीति निर्माण के दृष्टिकोण (Perspective) से ऐतिहासिक महत्व (Historical Importance) रखती है।
भारत में जनगणना का परिचय (Introduction to Census in India)
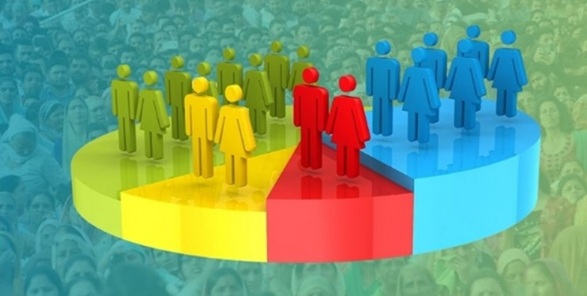
भारत में जातिगत जनगणना: ऐतिहासिक क्रम (Caste Census in India: Historical Timeline)
- 1872 – ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास हुआ।
- यह अखिल भारतीय (All-India) स्तर पर संगठित नहीं थी, बल्कि प्रारंभिक प्रयोग (Preliminary Experiment) था।
- इसमें जाति (Caste) के आंकड़े सीमित रूप में एकत्र किए गए।
- 1881 – लॉर्ड रिपन (Lord Ripon) के शासनकाल में पहली नियमित और संगठित जनगणना संपन्न हुई।
- यह जनगणना जातिगत वर्गीकरण (Caste-Based Classification) को केंद्र में रखकर आयोजित की गई थी।
- उद्देश्य: प्रशासन (Administration) को समाज के विभाजन के आधार पर शासन में सुविधा प्रदान करना।
- 1931 – अंतिम बार व्यापक जातिगत जनगणना हुई।
- इसमें सभी जातियों के सामाजिक (Social), आर्थिक (Economic) और जनसंख्या (Population) संबंधी आंकड़े शामिल थे।
- आज भी यह आंकड़े कई नीतिगत बहसों (Policy Debates) और अनुसंधान (Research) में संदर्भ (Reference) के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
- 1941 – जातिगत जानकारी सीमित रूप में संकलित (Compiled) की गई।
- आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) और प्रशासनिक चुनौतियों (Administrative Challenges) के कारण।
स्वतंत्र भारत में जातिगत आंकड़े
- 1951 – स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना।
- जातिगत आंकड़े केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) तक सीमित रहे।
- अन्य जातियों (Other Castes) की गणना नहीं की गई।
- 1990 – मण्डल आयोग (Mandal Commission) की सिफारिश के अनुसार सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया।
- इस निर्णय ने जातिगत आंकड़ों के महत्व को और अधिक बढ़ाया।
- 2011 – सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC – Socio-Economic and Caste Census)
- ऐतिहासिक पहल (Historic Initiative) के तहत आर्थिक स्थिति के साथ-साथ जातिगत आंकड़े भी देशभर में एकत्र किए गए।
- हालांकि, जातिगत डेटा अब तक सार्वजनिक (Public) नहीं किया गया।
- सरकार ने तकनीकी त्रुटियों (Technical Errors) और आंकड़ों की शुद्धता (Data Accuracy) पर सवालों के कारण इसे सार्वजनिक करने से परहेज़ किया।
- 2021- में निर्धारित जनगणना कोविड-19 महामारी (Pandemic) के कारण स्थगित (Postponed) कर दी गई थी।
- जातिगत जनगणना, सामान्य जाति-रहित जनगणना से भिन्न होती है।
- इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जाति की जानकारी (Caste Information) एकत्र की जाती है, जो नीति निर्माण, आरक्षण (Reservation) और सामाजिक न्याय (Social Justice) के लिए आवश्यक है।
संवैधानिक और कानूनी प्रावधान (Constitutional and Legal Provisions)
1. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)
- अनुच्छेद 246 (Article 246): संघ सूची (Union List) का विषय है, जिसमें जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है।
- सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule): प्रविष्टि 69 (Entry 69) में संघ सूची में जनगणना का उल्लेख।
- अनुच्छेद 340 (Article 340): राष्ट्रपति (President) द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes – SEBC) की स्थिति की जांच के लिए आयोग (Commission) गठित करने का प्रावधान।
2. कानूनी प्रावधान (Legal Provisions)
- जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) – दशकीय जनगणना का कानूनी आधार।
- जनगणना नियमावली, 1990 (Census Rules, 1990) – डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को विनियमित (Regulate) करती है।
जातिगत जनगणना की आवश्यकता (Need for Caste Census)
1. संवैधानिक अनुपालन (Constitutional Compliance)
- जातिगत जनगणना अनुच्छेद 340 और अन्य प्रावधानों के अनुरूप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान सुनिश्चित करेगी।
2. नीति निर्माण (Policy Making)
- जाति आधारित अद्यतन डेटा (Updated Data) नीति निर्माण (Policy Formulation) में साक्ष्य-आधारित (Evidence-Based) निर्णयों को सक्षम करेगा।
- कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) का लक्षित (Targeted) वितरण और संसाधनों का न्यायसंगत (Equitable) आवंटन।
3. सकारात्मक उपाय (Affirmative Action)
- आरक्षण के लाभार्थियों (Beneficiaries of Reservation) की सही पहचान।
- OBC (Other Backward Classes) के उप-वर्गों (Sub-Categories) में लाभ का समान वितरण।
- 2017 में गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग (Justice Rohini Commission) की रिपोर्ट उप-जातियों के लाभ वितरण को समर्थन करती है।
4. समुदायों की वास्तविक स्थिति समझना (Understanding Social Reality)
- महाराष्ट्र के मराठा (Marathas), हरियाणा के जाट (Jats) जैसे समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति।
- राष्ट्रीय संसाधनों पर उनके दावों (Claims) के उचित निर्णय में सहायता।
जातिगत सर्वेक्षण बनाम जातिगत जनगणना (Caste Surveys vs. Caste Census)
- सर्वेक्षण (Survey) सीमित अवधि और क्षेत्र के लिए होता है।
- जनगणना (Census) संविधान द्वारा वैधानिक (Statutory) प्रक्रिया है और पूरे देश में लागू होती है।
जातिगत जनगणना से जुड़ी चिंताएं (Concerns Related to Caste Census)
1. डेटा की सटीकता (Accuracy of Data)
- 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) में दोहरी प्रविष्टि (Duplicate Entries) और वर्तनी अशुद्धियाँ (Spelling Errors) हुईं।
- यदि अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण (Proper Training) नहीं मिलेगा तो त्रुटियाँ और जानबूझकर गलत प्रविष्टियाँ (Deliberate Misreporting) होने की संभावना।
2. वर्गीकरण (Classification Issues)
- केंद्र और राज्य की जाति सूचियों में अंतर।
- उदाहरण: हरियाणा में जाट OBC सूची में नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश में शामिल।
3. राजनीतिक संवेदनशीलता (Political Sensitivity)
- जातिगत डेटा पहचान आधारित राजनीति (Identity Politics) को बढ़ावा दे सकता है।
- जातियों द्वारा आरक्षण की मांग और सामाजिक अशांति (Social Unrest) संभव।
4. निजता और डेटा सुरक्षा (Privacy and Data Security)
- डिजिटल माध्यम (Digital Medium) से डेटा संग्रह में सुरक्षा जोखिम (Security Risk)।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) से गलत डेटा प्रविष्टि की संभावना।
जातिगत जनगणना की सफलता के उपाय (Measures for Successful Census)
1. परामर्श प्रक्रिया (Consultative Process)
- महारजिस्ट्रार (Registrar General) और जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) को विशेषज्ञ, जातीय समूहों, राजनीतिक संगठन और आम जनता से सलाह (Consultation) लेनी चाहिए।
2. राष्ट्रीय जाति निर्देशिका (National Caste Directory)
- मानकीकृत (Standardized) सूची तैयार करना।
- ऑनलाइन फीडबैक (Online Feedback) के माध्यम से सुधार और अंतिम रूप देना।
3. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (Training and Capacity Building)
- अधिकारियों और कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स (Big Data Analytics) का उपयोग।
4. आधुनिक तकनीक का प्रयोग (Use of Modern Technology)
- डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platforms) और मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile Applications) से डेटा संग्रह।
- डेटा की वास्तविकता और गुणवत्ता (Data Quality) सुनिश्चित करना।
जातिगत डेटा का महत्व (Significance of Caste Data)
- सामाजिक सुधार (Social Reforms) – डॉ. अंबेडकर के शब्दों में: “सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक सुधार संभव नहीं है”.
- समान अवसर (Equal Opportunities) – पिछड़े और हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए।
- नीति और योजना (Policy and Planning) – कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी और न्यायसंगत वितरण।
- OBC उप-वर्गीकरण (OBC Sub-Categorization) – लाभ का सही वितरण।
- साक्ष्य-आधारित निर्णय (Evidence-Based Decisions) – आरक्षण और कल्याण नीतियों का आधार।

 Contact Us
Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757
New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757
Tech Support : 9555124124/ 7428085757