| UPSC Mains GS–II (Governance, Polity, Welfare, Human Rights) GS–I (Modern Indian Society & Social Issues) |
हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) भारत की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार ढांचे और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह मानव गरिमा, न्याय और पुलिस/जेल प्रशासन की जवाबदेही से गहराई से जुड़ा विषय है। अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी के बावजूद, हिरासत में घटने वाली मौतें यह संकेत देती हैं कि भारत में सुरक्षा तंत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है।
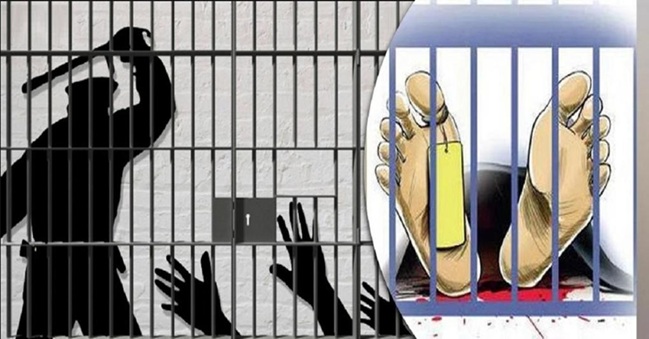
हिरासत में मृत्यु की परिभाषा और प्रकार
(A) पुलिस हिरासत में मृत्यु
गिरफ्तारी, पूछताछ, संक्रमण, यातना, अवैध निरोध या मेडिकल लापरवाही के दौरान।
(B) न्यायिक हिरासत में मृत्यु
जेल में बीमारी, आत्महत्या, हिंसा, भीड़भाड़, दवाइयों की कमी, मानसिक तनाव आदि के कारण।
हिरासत में यातना — प्रमुख कारण
- पुलिस द्वारा बलपूर्वक स्वीकारोक्ति पर निर्भरता
- Anti-Torture कानून का अभाव
- जेलों की भीड़भाड़ और चिकित्सा सुविधाओं की कमी
- स्वतंत्र जांच एजेंसियों का अभाव
- CCTV और तकनीकी निगरानी का अभाव
- वकील, कानूनी सहायता की कमी
- सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का दमन
भारत में हिरासत में मृत्यु — आँकड़े और वास्तविक स्थिति
- 2023 में कुल 1,754 हिरासत में मौतें (जेलों में)
- (सुप्रीम कोर्ट के Centre for Research & Planning के अनुसार)
- 1,237 से अधिक मामलों की पूछताछ एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित
- जो न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और जवाबदेही के संकट को दर्शाता है।
- 2016–2022 के बीच 11,656 कुल हिरासत में मौतें (संसद में दिए आँकड़े)।
- भारत UNCAT पर 1997 में हस्ताक्षर कर चुका है, परन्तु अब तक ‘अनुसमर्थन’ (Ratification) नहीं हुआ।
- इस कारण यातना को अपराध बनाने हेतु कोई मजबूत राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में नहीं आया।
हिरासत में यातना रोकने हेतु महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
(1) परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2020)
यह अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है।
निर्देश:
- NIA, CBI, पुलिस थानों सहित सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में CCTV लगाना अनिवार्य।
- CCTV में नाइट विज़न, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्टोरेज जैसी सुविधाएँ अनिवार्य।
- राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियाँ बनाना अनिवार्य।
- यह समितियाँ 2018 के Central Oversight Body (COB) की तर्ज पर गठित होंगी।
- CCTV का रखरखाव, कार्यशीलता और रिपोर्टिंग समितियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
इससे पुलिस पारदर्शिता और हिरासत में यातना की रोकथाम को मजबूत आधार मिला।
(2) डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)
भारत में ‘Human Rights Jurisprudence’ का आधार स्तम्भ।
मुख्य दिशा-निर्देश:
- गिरफ्तारी मेमो
- परिवार को सूचना
- 24 घंटे में मेडिकल जांच
- वकील का अधिकार
- डायरी एंट्री, थाने का पंजीकरण
- हिरासत में हिंसा रोकने हेतु SOP
(3) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)
- प्रत्येक राज्य में Police Complaints Authority की स्थापना
- SP और उच्च रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की स्वतंत्र जांच
(4) शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश (2018)
- गृह मंत्रालय को ‘Central Oversight Body’ (COB) बनाने का निर्देश
- अपराध स्थल की पूर्ण वीडियोग्राफी अनिवार्य
भारत में हिरासत में यातना से जुड़े सुरक्षा उपाय
आपके सभी प्रावधान नीचे व्यवस्थित किए जा रहे हैं:
(A) संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 14:-कानून के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 20(3):-स्वयं को दोषी ठहराने (Self-Incrimination) के खिलाफ सुरक्षा
- अनुच्छेद 21:-जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 22:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए, उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार हो और उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।
यह निवारक निरोध के मामलों पर भी लागू होता है, जिसमें कुछ अतिरिक्त नियम हैं, जैसे कि तीन महीने से अधिक की हिरासत के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है।
(B) NHRC के दिशा-निर्देश (1993)
- हिरासत में मृत्यु/बलात्कार की 24 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग अनिवार्य
- पोस्ट-मार्टम, फोटोग्राफी, मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य
- compensation और जवाबदेही प्रक्रिया
सरकार के प्रयास और तकनीकी सुधार
- CCTV अनिवार्यता (SC 2020 Judgement)
- स्मार्ट पुलिसिंग (SMART Police Model)
- Model Police Act 2006
- Prison Reforms Committee (Mulla Committee, Krishna Iyer Committee)
- Fast-Track Courts for custodial offences
- Forensic-based Investigation
- Police Training in Human Rights
चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं
- राज्यों में CCTV अब भी 100% functional नहीं
- Police Complaint Authorities निष्क्रिय
- Torture Prevention Law नहीं
- Undertrial कैदियों की संख्या बहुत अधिक
- जेलों की भीड़भाड़
- राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस पर दबाव
- पुलिसकर्मियों की कमी, लंबी ड्यूटी, तनाव
- फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर
आगे की राह: क्या किया जाना चाहिए ?
- Torture Prevention Law लागू करना → UNCAT का ratification
- 100% CCTV, Body Cameras, Interrogation Room Monitoring
- Independent Police Complaints Authority को शक्तिशाली बनाना
- Forensic-based Investigation को अनिवार्य करना
- पुलिस प्रशिक्षण में मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों को शामिल करना
- Undertrial कैदियों की रिहाई → Bail as Norm
- Jail Infrastructure सुधारना
- Accountability + Time-bound Investigation
निष्कर्ष
हिरासत में मृत्यु सिर्फ एक कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता, मानव गरिमा और न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा विषय है। जब तक पुलिस सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी निगरानी (CCTV, वीडियो रिकॉर्डिंग) मजबूत नहीं होंगे—भारत में हिरासत में मृत्यु की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। भारत को चाहिए कि वह UNCAT का अनुसमर्थन, कठोर कानून, स्वतंत्र निगरानी तंत्र और मानवाधिकार-आधारित पुलिसिंग मॉडल अपनाए। तभी ‘अनुच्छेद 21 — जीवन की गरिमा’ वास्तव में अर्थपूर्ण हो पाएगा।



