“यदि जल है, तो कल है — और यदि समाज जागरूक है, तो जल सुरक्षित है।”
भारत में जल संकट आज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगीकरण और जलवायु-परिवर्तन ने जल-संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।
ऐसे में केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं — स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ही स्थायी समाधान है।
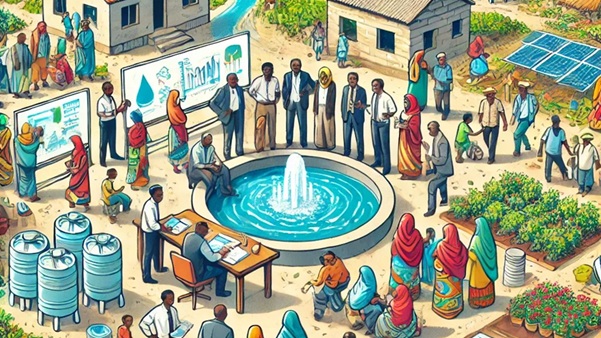
भारत में जल संकट की स्थिति
|
संकेतक
|
स्थिति
|
|
प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (1951)
|
5177 घन मीटर/वर्ष
|
|
प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (2025)
|
~1400 घन मीटर/वर्ष
|
|
भारत की जनसंख्या का हिस्सा
|
विश्व का 18%
|
|
जल संसाधनों का हिस्सा
|
विश्व का केवल 4%
|
|
भूजल दोहन
|
विश्व में सर्वाधिक (~25%)
|
- भारत “जल तनाव (Water Stress)” की स्थिति में है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, 700 से अधिक ब्लॉक “गंभीर या अति-शोषित” श्रेणी में हैं।
समुदाय आधारित जल संरक्षण क्यों आवश्यक ?
(1) स्थानीय ज्ञान और परंपराएँ
- ग्रामीण भारत में सदियों से वर्षा-जल संचयन, तालाब, बावड़ी, जोहड़, आहर-पइन जैसी प्रणालियाँ थीं — जो सामुदायिक सहयोग से चलती थीं।
(2) स्वामित्व की भावना
- जब लोग स्वयं योजना का हिस्सा बनते हैं, तो जल स्रोतों की रक्षा और रख-रखाव के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता है।
(3) विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन
- स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से योजनाएँ स्थानीय भूगोल, संस्कृति और जरूरतों के अनुकूल बनती हैं।
(4) सरकारी योजनाओं की सीमाएँ
- केवल टॉप-डाउन योजनाएँ (ऊपर से नीचे) अक्सर स्थानीय स्तर पर असफल रहती हैं यदि समुदाय की सहमति और भागीदारी न हो।
समुदाय आधारित जल संरक्षण के प्रमुख मॉडल (Models of Community Participation)
(1) राजस्थान का जोहड़ मॉडल – राजेन्द्र सिंह (Waterman of India)
- अलवर जिले में गाँव-गाँव जोहड़ (छोटे तालाब) बनाकर सूखे क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया।
- नदी अर्जुनी और रूपारेल फिर से बहने लगीं।
- यह “जन-सहभागिता से जल पुनर्जीवन” का आदर्श उदाहरण है।
(2) महाराष्ट्र का “पानी पंचायत” मॉडल
- 1980 के दशक में शुरू हुआ।
- सिद्धांत: “समान जल-वितरण और सामूहिक निर्णय”।
- किसान समूहों ने जल वितरण और सिंचाई में सामाजिक समानता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
(3) गुजरात का “Sardar Patel Participatory Water Conservation Program”
- चेक-डैम निर्माण में किसानों, NGOs और सरकार की साझेदारी।
- हजारों गाँवों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि।
(4) हिमालयी राज्य – चाल-खाल और नौला प्रणाली
- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में समुदाय स्वयं जलस्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण और पुनर्भरण कार्य करते हैं।
(5) दक्षिण भारत – Kudimaramathu (तमिलनाडु)
- प्राचीन परंपरा जिसमें ग्रामीण स्वयं अपने जलाशयों की मरम्मत करते थे; सरकार अब इसे पुनर्जीवित कर रही है।
नीति और संस्थागत प्रयास (Policy & Institutional Initiatives)
|
नीति / योजना
|
समुदाय से जुड़ा प्रावधान
|
|
जल शक्ति अभियान (2019)
|
“जन आंदोलन से जन भागीदारी” पर बल; कैच द रेन (Catch the Rain) अभियान।
|
|
अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana)
|
समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन; पंचायतों को योजना, कार्य और मॉनिटरिंग में शामिल किया गया।
|
|
मनरेगा (MGNREGA)
|
जल संरक्षण संरचनाएँ जैसे तालाब, नाला-बांध, चेक-डैम आदि — श्रमदान और जनभागीदारी से।
|
|
जल जीवन मिशन (JJM)
|
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप जल कनेक्शन — ग्राम जल समितियाँ इसका संचालन करती हैं।
|
|
राष्ट्रीय जल नीति (2023 का मसौदा)
|
सामुदायिक और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों के पुनर्जीवन पर बल।
|
समुदाय आधारित जल संरक्षण के लाभ (Benefits)
- जल संसाधनों का सतत उपयोग– सामूहिक नियंत्रण से अत्यधिक दोहन पर अंकुश लगता है।
- पर्यावरणीय पुनर्जीवन– जल स्रोतों के पुनर्भरण से वनस्पति, जीव और भूमि उत्पादकता बढ़ती है।
- सामाजिक एकता और सशक्तिकरण– पंचायत, महिला समूह, किसान समूह — सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया मजबूत होती है।
- आर्थिक लाभ– जल-सुलभता से कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय दोनों बढ़ते हैं।
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद– वर्षा-जल संचयन और सूखे की तैयारी में स्थानीय समुदायों की भूमिका निर्णायक।
प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges)
|
समस्या
|
विवरण
|
|
सामाजिक असमानता
|
जल संसाधनों पर प्रभुत्व सम्पन्न वर्गों का नियंत्रण; गरीब वर्ग की भागीदारी सीमित।
|
|
तकनीकी ज्ञान की कमी
|
कई बार पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उचित संयोजन नहीं हो पाता।
|
|
स्थायी वित्तीय संसाधन का अभाव
|
परियोजनाएँ आरंभ तो होती हैं पर दीर्घकालीन रख-रखाव में कमी।
|
|
सरकारी सहयोग की अनियमितता
|
योजनाओं की निरंतरता व नीति-समन्वय का अभाव।
|
|
शहरी क्षेत्रों में भागीदारी का अभाव
|
नगर स्तर पर नागरिकों की जल-संरक्षण में भूमिका अभी सीमित है।
|
आगे की दिशा (Way Forward)
- ‘जल पंचायतें’ और ‘जल उपयोगकर्ता संघ’ (Water User Associations) का विस्तार — स्थानीय निर्णयों को मान्यता दी जाए।
- महिला भागीदारी सुनिश्चित करना — जल प्रबंधन में महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावी हितधारक हैं।
- तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण — GIS, सेंसर, रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग के साथ स्थानीय पद्धतियाँ।
- शिक्षा और जनजागरूकता अभियान — स्कूल स्तर से जल साक्षरता (Water Literacy)।
- प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Incentive Mechanism) — ग्रामों को जल संरक्षण में उपलब्धि पर पुरस्कार।
- नागरिक-आधारित शहरी पहलें — सोसाइटी/अपार्टमेंट स्तर पर ग्रे-वाटर रीसायकल और रेनवॉटर सिस्टम अनिवार्य।
- नदियों की पुनर्जीवन परियोजनाएँ — जैसे “Rejuvenation of River Ganga” में ग्राम स्तर की निगरानी समिति।
निष्कर्ष (Conclusion)
- “जल का संरक्षण सरकार नहीं, समाज की साझेदारी से संभव है।”
- भारत के प्राचीन दर्शन में “नदी-देवता”, “तालाब-देवता” जैसे रूपों ने जल को पवित्र माना।
आज उसी भावना को आधुनिक नीति-निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता है।
- समुदाय-आधारित जल प्रबंधन = स्थानीय ज्ञान + सामाजिक सहयोग + वैज्ञानिक नीति
- यदि प्रत्येक गाँव, वार्ड और नगर अपने स्तर पर जल-संरक्षण की जिम्मेदारी ले, तो भारत 2047 तक “जल आत्मनिर्भर राष्ट्र” (Water Secure India) बन सकता है।



