भारत में जल-प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल — सब पर औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और रासायनिक पदार्थों का बढ़ता बोझ है। इसी समस्या से निपटने के लिए 1974 में “जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम” लाया गया था। साल 2024 में इसमें एक बड़ा संशोधन अधिनियम लाया गया है, जिसका उद्देश्य है —
“जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, प्रभावी और ‘Ease of Doing Business’ के अनुकूल बनाना।”
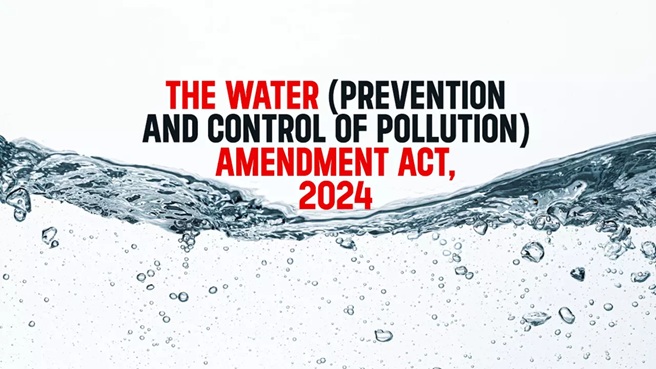
पृष्ठभूमि (Background)
(क) मूल अधिनियम – 1974
- यह अधिनियम संसद द्वारा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत पारित किया गया था।
- इसका लक्ष्य था: जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, और जल की शुद्धता बनाए रखना।
- इसके अंतर्गत स्थापित किए गए:
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)
- औद्योगिक इकाइयों को किसी भी जल-स्रोत में अपशिष्ट या अपवाह छोड़ने से पहले अनुमति (Consent) लेना आवश्यक था।
- उल्लंघन पर कैद और जुर्माने का प्रावधान था।
(ख) संशोधन की आवश्यकता
- पिछले 50 वर्षों में औद्योगिक ढांचा, पर्यावरणीय चुनौतियाँ और तकनीक काफी बदल चुकी हैं।
- अनेक मामलों में केवल तकनीकी चूक या रिपोर्टिंग-विलंब के लिए भी आपराधिक सजा होती थी।
- यह न तो प्रभावी रोकथाम करता था, न ही निवेश को प्रोत्साहित करता था।
- कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में कर्मियों व तकनीकी क्षमता की कमी थी।
- इसी परिप्रेक्ष्य में 2024 का संशोधन अधिनियम लाया गया — ताकि तंत्र अधिक सक्षम, दंड-मुखी से अनुपालन-मुखी (compliance-driven) बने।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)
(1) क्षेत्रीय लागू क्षेत्र (Territorial Application)
- संशोधित अधिनियम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासित प्रदेशों में तुरंत लागू हुआ।
- अन्य राज्य इसे अनुच्छेद 252 के तहत अपनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं।
- उदाहरण: बिहार ने अप्रैल 2025 में इसे अपनाने की अधिसूचना जारी की।
(2) केंद्र की भूमिका सशक्त (Empowerment of Central Government)
- नई धारा 27A जोड़ी गई है: केंद्र सरकार, CPCB के परामर्श से, राज्य बोर्डों के ‘अनुमति-प्रक्रिया’ संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
- यह एकरूपता सुनिश्चित करेगा — ताकि देशभर में मानक समान हों।
(3) दंड प्रावधानों में बड़ा परिवर्तन (Decriminalisation)
- पहले कई उल्लंघनों पर कैद (जेल) का प्रावधान था।
- अब अधिकांश तकनीकी या प्रथम बार के उल्लंघनों को जुर्माने योग्य अपराध घोषित किया गया है।
- दंड राशि:
- ₹10,000 से लेकर ₹15 लाख तक
- पुनरावृत्ति पर अधिक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- उद्देश्य: “सजा नहीं, बल्कि अनुपालन को प्रोत्साहन”।
(4) औद्योगिक इकाइयों को छूट (Exemptions)
- केंद्र सरकार अब कुछ कम-जोखिम वाले उद्योगों को ‘अनुमति लेने की बाध्यता’ से छूट दे सकती है।
- यह उद्योगों की श्रेणी CPCB के परामर्श से तय की जाएगी।
- इससे ‘Ease of Doing Business’ में सुधार की उम्मीद है।
(5) दंड निर्धारण प्रक्रिया के नए नियम
- “जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (दंड निर्धारण प्रक्रिया) नियम, 2024” अधिसूचित किए गए हैं।
- इसमें यह तय किया गया है कि जाँच, सुनवाई, दंड निर्धारण आदि किस प्रकार होंगे।
- यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने का प्रयास है।
अधिनियम का महत्व (Significance)
(1) शासन सुधार की दिशा में कदम
- अपराधीकरण-रहित व्यवस्था से न्यायालयों पर बोझ घटेगा।
- जुर्माने-आधारित प्रणाली से त्वरित समाधान संभव।
(2) व्यवसायिक वातावरण में सुधार
- छोटे-मोटे उल्लंघनों में जेल का भय खत्म — जिससे उद्योगों को राहत।
- “Ease of Doing Business” और “Make in India” को बल मिलेगा।
(3) पर्यावरणीय नियमन में एकरूपता
- केंद्रीय दिशा-निर्देशों से राज्यों में समान मानक और नीतिगत स्पष्टता।
(4) सार्वजनिक हित और जल गुणवत्ता
- बेहतर अनुपालन से नदियों-तालाबों की गुणवत्ता सुधरेगी, जनस्वास्थ्य में सुधार होगा।
आलोचनाएँ एवं चुनौतियाँ (Issues & Challenges)
(1) दंड-प्रभाव की कमजोरी
- कुछ विशेषज्ञों का मत है कि जुर्माने-प्रधान व्यवस्था से भय-कारक (deterrence) कम हो सकता है।
- यदि जुर्माना उद्योगों के लाभ की तुलना में बहुत छोटा हो, तो वे इसे “व्यवसाय की लागत” मान सकते हैं।
(2) राज्यों की भूमिका कमजोर होना
- जल विषय संविधान की राज्य सूची (Entry 17, List II) में है।
- केंद्र के बढ़ते नियंत्रण से संघ-राज्य संतुलन पर प्रश्न उठ सकते हैं।
(3) राज्यों की क्षमता सीमाएँ
- अधिकांश SPCB के पास पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता, प्रयोगशालाएँ व कर्मी नहीं हैं।
(4) कार्यान्वयन का अभाव
- कानून अच्छा है, परंतु जमीनी निगरानी, डेटा-साझाकरण और पारदर्शिता न हो तो प्रभाव सीमित रहेगा।
(5) छूट-नीति का जोखिम
- यदि “कम-जोखिम उद्योग” की परिभाषा बहुत उदार रखी गई तो यह कुल प्रदूषण भार बढ़ा सकता है।
आगे की राह (Way Forward)
|
सुधार क्षेत्र
|
सुझाव
|
|
संस्थागत क्षमता
|
SPCB व CPCB को आधुनिक तकनीक (IoT आधारित सेंसर, GIS मॉनिटरिंग) और पर्याप्त स्टाफ से लैस करें।
|
|
पारदर्शिता
|
सभी अनुमति, छूट व दंड-सूचना को सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए।
|
|
दंड-प्रणाली
|
दोहराए जाने वाले उल्लंघनों पर जुर्माना कई गुना बढ़ाया जाए।
|
|
सामाजिक भागीदारी
|
स्थानीय समुदायों, NGOs और नागरिकों को निगरानी में शामिल किया जाए।
|
|
राज्यों का समन्वय
|
सभी राज्यों को शीघ्र अधिनियम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
|
|
आवधिक समीक्षा
|
2-3 वर्ष बाद इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए।
|
निष्कर्ष (Conclusion)
“यह अधिनियम केवल कानून में संशोधन नहीं, बल्कि पर्यावरणीय शासन-दर्शन में परिवर्तन है।”
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 भारत की पर्यावरणीय नीतियों के आधुनिकीकरण का प्रतीक है। यह आपराधिक-दंड आधारित व्यवस्था को प्रशासनिक-दंड आधारित प्रणाली में बदलता है — ताकि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों संतुलित रहें।
कानून तभी सफल होगा जब:
- केंद्र-राज्य सहयोग मजबूत हो,
- प्रवर्तन निष्पक्ष हो,
- और जनता इस प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बने।



