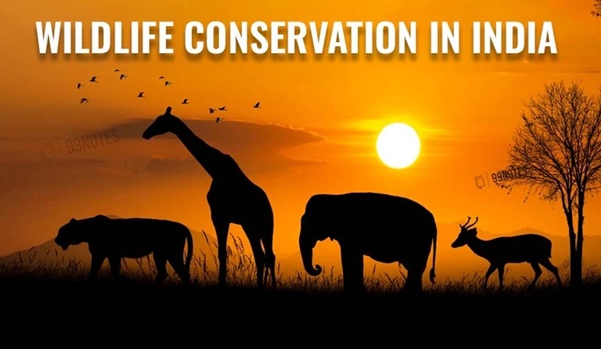भारत जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। यहां लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है — जिसमें स्तनधारियों की 7%, पक्षियों की 12%, उभयचरों की 6% और पुष्पीय पौधों की लगभग 6% प्रजातियां शामिल हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में भारत में वन्यजीव संरक्षण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।
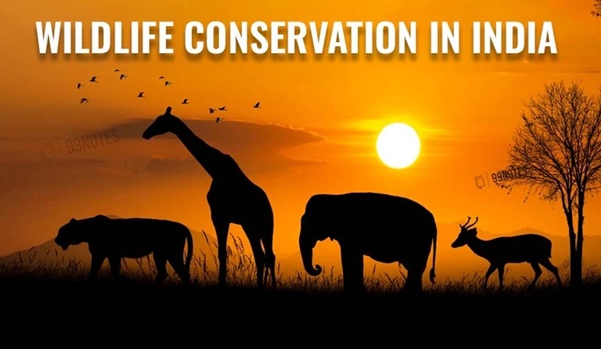
भारत में वन्यजीव संरक्षण पर संवैधानिक और संस्थागत ढांचा (Constitutional & Institutional Framework)
1. संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions):
- अनुच्छेद 48A (राज्य की नीति के निदेशक तत्व): राज्य को पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51(A)(g) (मौलिक कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन, झील, नदी और जीव-जंतुओं की रक्षा करे।
- 7वीं अनुसूची (समवर्ती सूची): ‘वन’ और ‘संरक्षण’ विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी हैं।
कानूनी ढांचा (Legal Framework)
1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:
- वन्यजीव संरक्षण हेतु मुख्य कानून।
- इसमें चार अनुसूचियां हैं — जो संरक्षण के स्तर के अनुसार प्रजातियों को वर्गीकृत करती हैं।
- उल्लंघन पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान।
- अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं —
- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks)
- वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries)
- संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserves)
- सामुदायिक रिजर्व (Community Reserves)
2. अन्य प्रमुख संस्थाएं:
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) — अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र
भारत में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (Protected Area Network in India)
- भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.32% हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों में आता है।
- नवंबर 2023 तक:
- 100+ राष्ट्रीय उद्यान
- 550 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य
- 100+ संरक्षण रिजर्व
- 200+ सामुदायिक रिजर्व
प्रमुख उपलब्धियां (Major Achievements)
1. बाघ संरक्षण (Project Tiger)
- 1973 में प्रारंभ हुआ और 2023 में 50 वर्ष पूरे हुए।
- भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हुई।
- भारत ने TX2 Initiative के तहत बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य 4 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया।
2. हाथी संरक्षण (Project Elephant)
- हाथियों की संख्या 2018 में 26,786 से बढ़कर 2022 में 29,964 हो गई।
- Elephant Corridors और Human-Elephant Conflict Management पर विशेष ध्यान।
3. प्रोजेक्ट चीता (2022)
- नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से एशियाई चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य विलुप्त प्रजातियों को पुनः भारतीय पारिस्थितिकी में स्थापित करना है।
4. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)
- भारत की पहल पर गठित एक अंतर-सरकारी संगठन।
- इसमें बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, जगुआर, स्नो लेपर्ड आदि के संरक्षण का लक्ष्य।
- मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा।
मुख्य चुनौतियां (Major Challenges)
|
चुनौती
|
विवरण
|
|
1. पर्यावास हानि (Habitat Loss)
|
WWF के अनुसार हर वर्ष लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाते हैं।
|
|
2. वन्यजीव अपराध (Wildlife Crime)
|
गैंडे, पैंगोलिन और हाथी सबसे अधिक प्रभावित।
|
|
3. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
|
तापमान में वृद्धि और वर्षा पैटर्न में बदलाव से प्रजातियों के आवास प्रभावित।
|
|
4. मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict)
|
जनसंख्या विस्तार और अवैध घुसपैठ से संघर्ष बढ़ा।
|
|
5. संक्रामक बीमारियां (Zoonotic Diseases)
|
लगभग 50% उभरती संक्रामक बीमारियां मनुष्य-प्राणी-पारिस्थितिकी तंत्र के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न (IPBES Report)।
|
|
6. जैव विविधता में गिरावट
|
WWF की Living Planet Report (2020) के अनुसार, 1970–2020 के बीच वन्यजीव आबादी में 73% गिरावट।
|
प्रमुख योजनाएं व पहलें (Key Schemes & Initiatives)
- वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats - IDWH)
- केंद्र प्रायोजित योजना।
- वन्यजीव गलियारे, बफर ज़ोन विकास, और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन।
- स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम
- संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे हंगुल, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, bustard आदि के संरक्षण हेतु।
- संरक्षण के लिए भू-परिदृश्य दृष्टिकोण (Landscape Approach)
- संरक्षण क्षेत्रों को गलियारों के माध्यम से जोड़कर जेनेटिक विविधता और प्रजनन व्यवहार्यता बनाए रखना।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)
- अवैध व्यापार व तस्करी की रोकथाम।
- NGO की भूमिका
- भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WWF इंडिया जैसी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी।
आगे की राह (Way Forward)
- समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल: स्थानीय समुदायों को संरक्षण के लाभों से जोड़ना।
- इको-टूरिज्म में संतुलन: पर्यटन दबाव घटाते हुए स्थानीय रोजगार सृजन।
- वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा आधारित नीति: WII और अन्य संस्थानों में आधुनिक डीएनए अनुक्रमण प्रयोगशालाएं विकसित करना।
- वन्यजीव गलियारे (Wildlife Corridors) मजबूत करना: ताकि प्रजातियों का प्राकृतिक प्रवास (migration) बना रहे।
- जलवायु अनुकूलन रणनीति: संवेदनशील क्षेत्रों में बफर ज़ोन को पुनः डिज़ाइन करना।
- सख्त प्रवर्तन: वन्यजीव अपराधों पर जीरो-टॉलरेंस नीति।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है — बाघ, हाथी, चीता जैसे कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर उदाहरण बने हैं। फिर भी, बढ़ती मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के बीच संरक्षण को “विकास के पूरक” के रूप में देखना आवश्यक है।
“वन्यजीवों की रक्षा केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की भी शर्त है।”

 Contact Us
Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757
New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757
Tech Support : 9555124124/ 7428085757